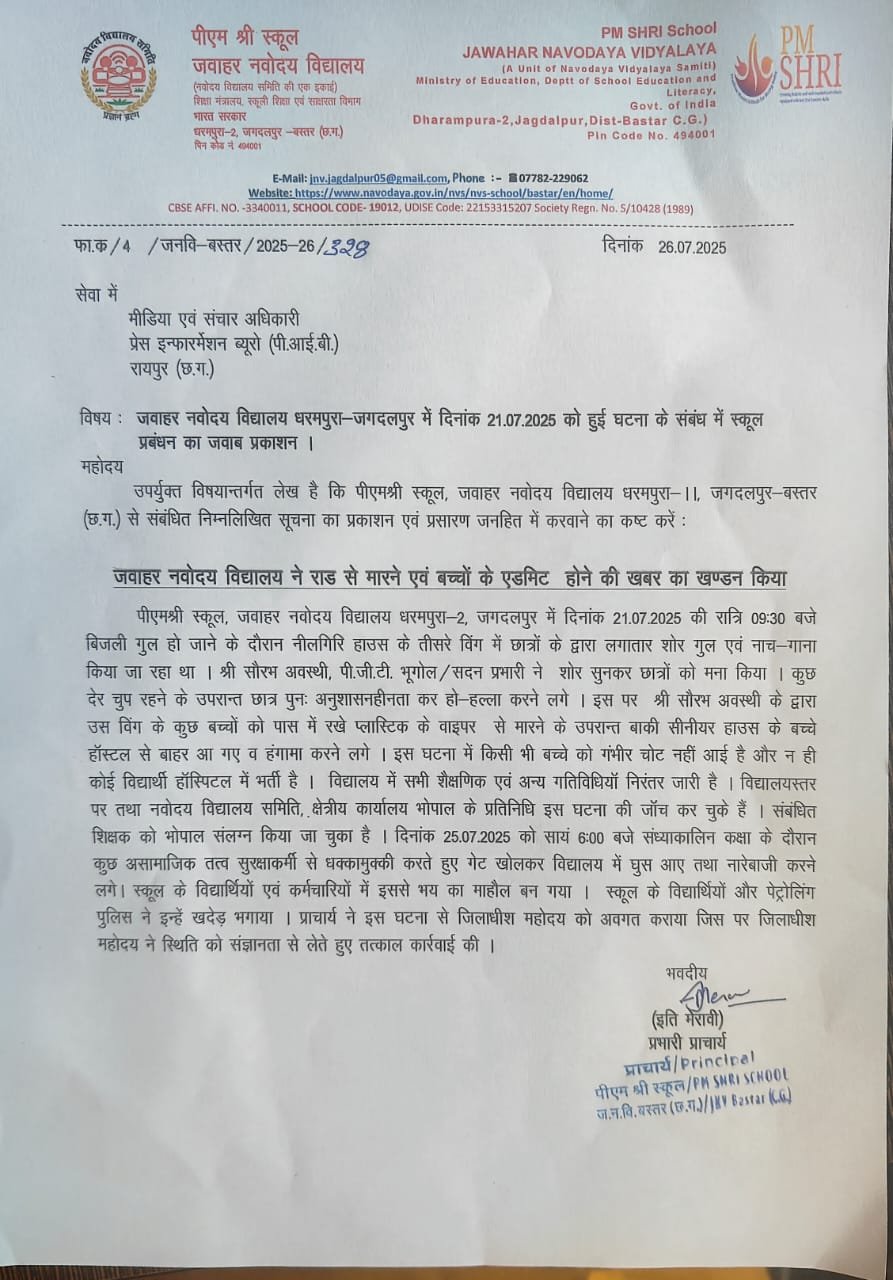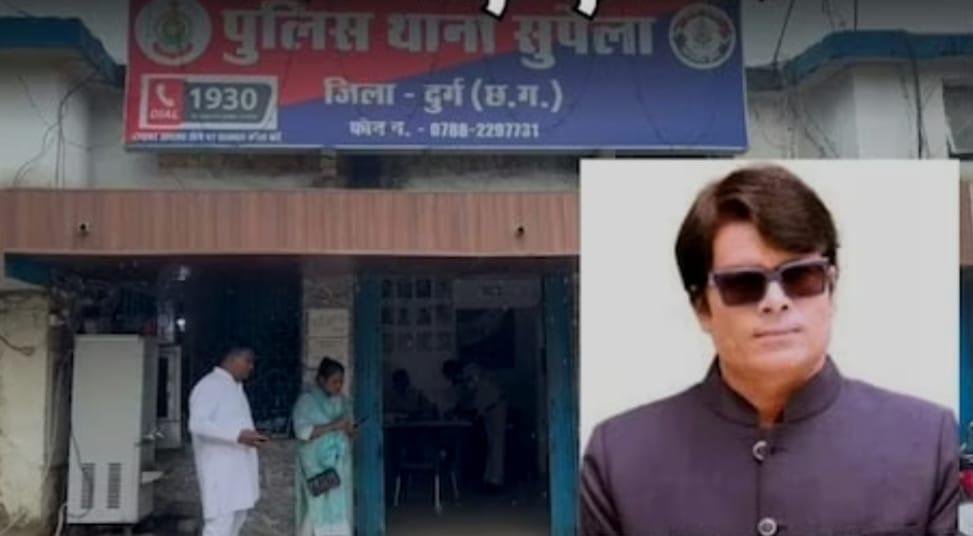पर्यावरण कुजनेट्स वक्र (एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व) से हासिल पर्यावरण के प्रशासन से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि देश पहले विकास करते हैं और बाद में सफाई में जुटते हैं। यह अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि अब विकसित हो चुके उन देशों के अनुभवों से प्रेरित है, जिन्होंने विकास की प्रक्रिया में संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु देश और विदेश में प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन किया। लेकिन ऐसी सुविधा भारत जैसे देशों को नसीब नहीं है, जिन्हें अपनी विशाल आबादी की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभी भी तेज गति से विकास करने की जरूरत है।
जब 2014 में एनडीए सत्ता में आई, तो चुनौती हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल सिद्धांतों – “सुधार, प्रदर्शन और बदलाव” – पर आधारित विकास एवं प्रगति को गति देने की थी। इन सिद्धांतों में जरूरत के हिसाब से पर्यावरण की सुरक्षा के सख्त उपायों से समझौता किए बिना ‘व्यवसाय करने में आसानी’ की सुविधा प्रदान करते हुए तेजी गति से विकास करना शामिल था। आज 2025 में, हम न सिर्फ इस चुनौती से निपट पाने में सफल रहे हैं बल्कि हमने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे सारी दुनिया ने माना है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था: इस प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदला जाए जो “इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था” दोनों के लिए फायदेमंद हो।
वर्ष 2014 में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की शुरुआत हमारी पहली बड़ी पहल थी। यह पहल स्वच्छता से आगे बढ़कर कचरे के प्रबंधन व पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने तक जा पहुंची। इस मिशन ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को सामाजिक विकास के साथ जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस मिशन को सभी नागरिकों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और एक स्वच्छ एवं संसाधन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक कुशल भारत की चाहत को आगे बढ़ाया गया था। विभिन्न शहरों में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी सुविधा प्रदान करने के तुरंत बाद राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया।
वर्ष 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल में भी कड़े पर्यावरण अनुपालन मानकों को शामिल किया गया। इससे यह साबित हुआ कि हम इकोलॉजी की स्थिरता को बनाए रखते हुए मैन्यूफैक्चरिंग को अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर और तेज गति से बढ़ावा दे सकते हैं। ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा पर आधारित अधिक संख्या में उद्योगों को शामिल करने के उद्देश्य से 2015 में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का विस्तार किया गया। इससे ऊर्जा संबंधी दक्षता के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र का निर्माण हुआ।
कचरे के कारगर प्रबंधन, संसाधन संबंधी दक्षता में बढ़ोतरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से कचरे के प्रबंधन के सभी प्रमुख नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का बुनियादी सिद्धांत बाजार आधारित तंत्र और “प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत” पर आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से जुड़े ढांचे पर निर्भरता में निहित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम तथा टायर, बैटरी एवं प्रयुक्त तेल अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए थे। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जिसके तहत विभिन्न सामग्रियों के लगभग 4,000 पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है। इस कदम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 61,055 उत्पादकों ने प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बेकार टायर, बैटरी के कचरे और प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में काम करने हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अपशिष्ट नियम, 2022 के प्रकाशन और ईपीआर पोर्टल की शुरूआत के बाद, शोधित अपशिष्ट की मात्रा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन नियमों के प्रकाशन से पहले 3.6 एमएमटी प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 127.48 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है। यह सभी हितधारकों के सहयोग एवं समर्थन से संभव हुआ है।
प्रक्रियागत देरी में कमी लाने और एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 2018 में ‘परिवेश’ (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरएक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरनमेंटल सिंगल-विंडो हब) नाम के एक ऑनलाइन आईटी टूल का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार करते हुए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यवसाय जगत और पर्यावरण नियामकों के बीच के संवाद में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। ‘परिवेश’ ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बोझिल एवं कागज-आधारित प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित एवं मजबूत डिजिटल अनुभव में बदल दिया है। इस दृष्टिकोण ने जहां पर्यावरण से जुड़े सख्त मूल्यांकन को बनाए रखा है, वहीं इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी ला दी है और पारदर्शिता को बढ़ाया है।
वर्ष 2019 में शहरों पर केन्द्रित कार्य योजनाओं से लैस ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (एनसीएपी) के आधिकारिक शुभारंभ ने हमें नीति निर्माता एवं नियामक से बदलकर अमल करने वाला बना दिया है। एनसीएपी का लक्ष्य 2025-26 तक पीएम10 सांद्रता में 40 प्रतिशत की कमी लाना या आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के राष्ट्रीय मानक को हासिल करना है। एनसीएपी के साथ-साथ सीपीसीबी ने एनसीएपी के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता के रुझान की बारीकी से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वायु की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हुई है। वर्ष 2021 में, गैर-प्राप्ति वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के नियमन हेतु पोर्टल (पीआरएएनए) को कागज रहित परियोजना प्रबंधन के एकल बिंदु वाले वेब-आधारित उपकरण के रूप में शुरू किया गया। इससे स्वच्छ वायु से जुड़े उपायों के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नजर रखना संभव हो सकेगा।
1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक शीट पर प्रतिबंध ने जहां पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया, वहीं उसी वर्ष शुरू किए गए ‘जल जीवन मिशन’ ने पानी की सुलभता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा।
एक व्यापक ‘भारत शीतलन कार्य योजना’ विकसित करके भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस कार्य योजना में विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण समावेश है तथा इसमें ऐसे कार्यों की सूची दी गई है, जो शीतलन से जुड़ी मांग को कम करने में सहायक हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन की जरूरत होती है तथा यह आर्थिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन, कोल्ड-चेन, प्रशीतन, परिवहन और उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जरूरत पड़ती है।
भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उत्सर्जन में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने हेतु 27 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का अनुमोदन किया। इसके तहत 2032 से आगे चार चरणों में चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और 2032, 2037, 2042 एवं 2047 में उत्सर्जन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 85 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
वर्ष 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना की। इससे उत्सर्जन में कमी से संबंधित बाजार आधारित तंत्र का निर्माण हुआ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत 2023 में हमारी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का संचालन देश के पहले व्यापक कार्बन बाजार के निर्माण की राह में एक अहम पड़ाव है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित ‘मिशन लाइफ’ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मानव व्यवहार को प्रेरित करके टिकाऊ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने वाला एक और अनुकरणीय कदम है।
कार्बन क्रेडिट के अलावा, ‘ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम’ के रूप में एक सकारात्मक उपाय की शुरुआत 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में सीओपी28 के दौरान की गई ताकि पर्यावरण से संबंधित सकारात्मक कार्यों को पुरस्कृत किया जा सके और स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रबंधन को प्रेरित करने वाले प्रोत्साहनों का सृजन किया जा सके।
वर्ष 2024 में देश भर में भारत स्टेज VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंडों का पूर्ण कार्यान्वयन और टिकाऊ वित्त हेतु हमारे हरित कर प्रणाली (ग्रीन टैक्सोनॉमी) के ढांचे का विकास ऐसे कदम हैं जो स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये कदम इस बात को भी दर्शाते हैं कि पर्यावरण से जुड़ा प्रशासन कैसे तकनीकी उन्नति और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
पर्यावरण के अनुकूल और गुणवत्ता वाले टिकाऊ उत्पादों के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने ई(पी) अधिनियम, 1986 के तहत इकोमार्क नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। इसमें उत्पादन और उपभोग की टिकाऊ पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादों की 80 उप-श्रेणियों के साथ 17 व्यापक श्रेणियां शामिल की गईं हैं और सीपीसीबी को प्रमुख प्रशासनिक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
वर्ष 2018 में ‘परिवेश’ के शुभारंभ से लेकर 2024 में ‘परिवेश 2.0’ तक का विकास, पर्यावरण संबंधी प्रबंधन एवं निगरानी की प्रक्रिया में निरंतर तकनीकी व गुणात्मक सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘परिवेश 2.0’ में जीआईएस से लैस एक आधुनिक निर्णय समर्थन प्रणाली और एक बेहतर पर्यावरणीय मूल्यांकन सुविधाओं का समावेश है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में पर्यावरण संबंधी मंजूरी को समन्वित करने से व्यवसाय संबंधी अनुमोदन का एक ‘वन-स्टॉप’ डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। इससे व्यवसाय करने में आसानी से जुड़ी विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत का स्थान की नाटकीय रूप से बेहतर हुआ। भारत इस रैंकिंग में 2014 में 142वें स्थान से उछलकर 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। वर्ष 2014-2020 के बीच, हमने 2,115 आवेदनों में से लगभग 2,053 परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी प्रदान की जिससे आवेदनों को निपटाने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
कचरे के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के उद्देश्य से, उद्योगों को वर्गीकृत करने की एक नई पद्धति शुरू की गई है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत विभिन्न गतिविधियों को लाल, नारंगी, हरे, सफेद और नीले रंग की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नीले रंग की नई श्रेणी वाले उद्योग सीवेज शोधन संयंत्र, खाद बनाने वाली इकाई, बायोगैस संयंत्र और सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति से जुड़ी सुविधा जैसे पर्यावरण के अनुकूल सकारात्मक उपायों से लैस होते हैं।
जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ा हमारा प्रशासकीय ढांचा उन्नत एआई क्षमताओं, उन्नत सार्वजनिक भागीदारी तंत्र और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से लैस होकर विकसित होता जा रहा है। उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली और ईएसजी रिपोर्टिंग की ठोस व्यवस्थाओं समेत 2025 में हुए हालिया विकास, अत्याधुनिक बने रहने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं।
लालफीताशाही से लेकर हरित रचनात्मकता तक की दशक भर की यह यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि एक दूरदर्शी नेतृत्व बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करता है।
अब जबकि हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, एक दशक से अधिक समय में लागू किया गया पर्यावरण से जुड़ा प्रशासकीय ढांचा टिकाऊ विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।